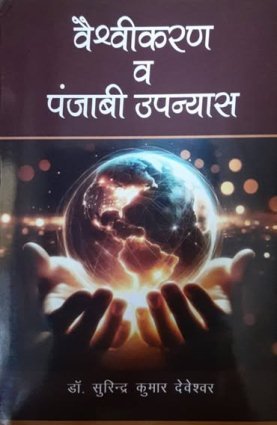
सुरेंद्र कुमार देवेश्वर की आलोचना पुस्तक ‘वैश्वीकरण व पंजाबी उपन्यास’ का आधार एक विमर्श जरूर है, तथापि एक अन्य अर्थ में हम इसे अपने आप में एक स्वतंत्र विमर्श भी कह सकते हैं।
वैश्वीकरण और पंजाबी उपन्यास : एक नई दृष्टि
विनोद शाही
सुरेंद्र कुमार देवेश्वर की आलोचना पुस्तक ‘वैश्वीकरण व पंजाबी उपन्यास’ का आधार एक विमर्श जरूर है, तथापि एक अन्य अर्थ में हम इसे अपने आप में एक स्वतंत्र विमर्श भी कह सकते हैं।
बात जब पंजाबी उपन्यास की है, तो यह मुमकिन ही नहीं के उसके तहत हम वैश्वीकरण की परिघटना के रूबरू खड़े नहीं होंगे। पंजाब भारत के ऐसे राज्यों में से एक है जो एक अरसे से बहुराष्ट्रीय होने की नियति की मार्फत ही, अपने इतिहास बोध को पाता रहा है। भौगोलिक रूप में पंजाब ऐसी जगह पर दिखाई देता है, जहां प्राचीन काल से ही उसकी सभ्यता और संस्कृति, विविध राष्ट्रों की विविध जातियों के संपर्क के भीतर से ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करती रही है।
वैदिक काल की बात हो, तो आर्य और अनार्य जातियों के सम्मिश्रण का इतिहास वहां पीछे खड़ा दिखाई देगा। मध्यकाल की बात होगी, तो भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण, बरास्ते सिंध, पंजाब की धरती से होते हुए, आगे बढ़ते दिखाई देंगे। और आधुनिक काल की बात हो, तो औपनिवेशिक दौर के हालात के बाद दो मुल्कों के रूप में होने वाले भारत के विभाजन के मानचित्र पर पंजाब और बंगाल ही प्रमुखता से अंकित दिखाई देंगे। ये सब मिलकर पंजाब को विविध राष्ट्रों के संगम-स्थल के रूप में निर्मित करने का आधार हो जाते हैं।
अब हम पंजाब में रचे जाने वाले उपन्यासों के परिदृश्य की ओर आ सकते हैं। बहुराष्ट्रीय मानसिकता को अपने इतिहास बोध की तरह जीने वाला यह पंजाब, आधुनिक काल में जब वैश्वीकरण के हालात के रूबरू होता है, तो इसी वजह से वह इस संदर्भ में सर्वाधिक संवेदनशील भी दिखाई देता है।
इसलिए देवेश्वर जब पंजाबी उपन्यास को वैश्वीकरण के आईने में देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो वह इस उपन्यास को समझने का एक बुनियादी और जरूरी विमर्श बन जाता है।
इस किताब को पढ़ते हुए हमें शुरू में यह लग सकता है कि हम किसी ऐसे वैश्वीकरण की प्रकृति और प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जनक पश्चिमी पूंजीवाद है। लेकिन फिर जल्द ही वे अपनी इस किताब को लिखने के असल सरोकार को हमारे सामने उद्घाटित करने लगा पड़ते हैं। इस सरोकार का संबंध, इस धारणा की छानबीन करने के साथ है की इस वैश्वीकरण को लेकर पंजाबी उपन्यास करता क्या है। तब हमें समझ में आने लगता है कि पंजाबी उपन्यास के मूल प्रकृति, सत्ता से प्रतिरोध के भीतर से खुद को खोजती है।
बेशक अपने अध्ययन में उन्होंने यह पाया है कि वैश्विक पूंजीवाद के बहुराष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण के एजेंडे के प्रतिरोध में, अनेक स्वर पश्चिम में भी लगातार उठाते दिखाई देते रहे हैं। तथापि हम इस अध्ययन से यह बात भी जल्द ही समझने लगते हैं कि पंजाबी उपन्यास का प्रतिरोध किस रूप में अलग और विशिष्ट है।
वैश्वीकरण अपने साथ मुक्त बाजार और पूंजी के कॉर्पोरेट तंत्र को साथ लाता है, सूचना तंत्र के जरिए अपने आप को दुनिया भर के लिए जरूरी बनाता है और आर्थिक असमानता को खड़ा करके दुनिया को अंतर विभाजित भी करता है। परंतु जहां तक भारत का और उसमें पंजाब जैसे राज्य का संबंध है, वहां वैश्वीकरण के मुनाफा वादी आत्म केंद्रित और अमानवीय रूप से सीधे लोहा लेने की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। बहुत कुछ है जहां भारत और उसके एक राज्य के रूप में पंजाब को, वैश्वीकरण की आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी विविध वित्तीय संस्थाओं की शर्तों को एक हद तक मानना पड़ता है। परंतु सांस्कृतिक स्तर पर हमारे यहां प्रतिरोध के अलग रूप उभरते भी दिखाई देते हैं। उनका संबंध हमारी सांस्कृतिक जमीन से है।
जैसे इस किताब में देवेश्वर इस विचार को हमारे सामने रखते हैं कि भारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समन्वित रूप वाले जिस विमर्श की जमीन मौजूद है वह मौजूदा वैश्वीकरण के अंतर विरोधों से एक हद तक निजात पाने में हमारी सहायता कर सकता है।
पंजाबी उपन्यास के इतिहास पर विचार करते हुए देवेश्वर ने पंजाब के पहले उपन्यास के रूप में नानक सिंह के ‘सुंदरी’ पर भी अलग तरह से विचार करने की जरूरत पर बोल दिया है। ईसाई मिशनरियों का प्रतिरोध करने के लिए जब हम अपनी सांस्कृतिक जमीन के मानवीय रूपों की तलाश में निकलते हैं, तो कांटे से कांटा निकालना की नीति के आधार पर हमें भी, एक हद तक सांप्रदायिक होने देखने का खतरा उठना पड़ता है।
औपनिवेशिक दौर में हमारे यहां पूंजीवाद का जो दासता मूलक रूप पनपता है, वह हमारा सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करना चाहता है। इसके साथ-साथ वह पश्चिमी संस्कृति के विस्तार के लिए उसे एक आधार की तरह इस्तेमाल भी करना चाहता है। यहां हम अपने व्यक्तित्व को सांस्कृतिक रूप में बचाने के लिए अपने तरह के रास्ते खोजते दिखाई देते हैं।
हालांकि कुछ उपन्यास ऐसे भी दिखाई देते हैं, जो पश्चिम की उपभोक्तावादी और मुक्त भोगवादी का ही अधिक अनुकरण करते प्रतीत होते हैं। वे इसे आधुनिक और उत्तर-आधुनिक होने का एक लक्षण मान लेते हैं। परंतु गहरे में ऐसा करते हुए भी हमारा उपन्यास अपनी तरह के मानवीय संबंधों की जमीन को खोजता अवश्य दिखाई देता रहता है। यह खोज भी एक तरह से वैश्वीकरण का मानवीय प्रतिरोध ही है।
इस तरह हम देख सकते हैं कि पंजाबी उपन्यास का वैश्वीकरण के नुक्ते-निगाह से किया गया यह अध्ययन, अपने आप में एक साहित्यिक विमर्श के रूप में भी खुद को मजबूती से खड़ा करता दिखाई देने लगता है। स्पष्ट है, पंजाबी उपन्यास को अधिक करीब से जानने समझने के लिए यह किताब एक जरूरी किताब की तरह है, जिसका स्वागत होना चाहिए।







